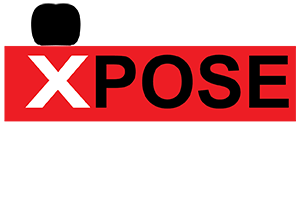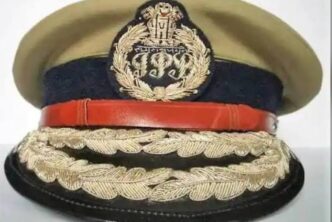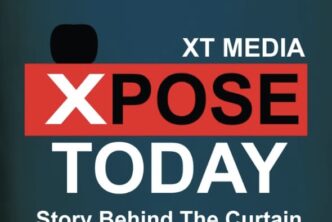ओमप्रकाश श्रीवास्तव
आईएएस अधिकारी एवं
धर्म, दर्शन और सहित्य के अध्येता
एक्सपोज़ टुडे।
इस वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि अर्थात् प्रतिपदा 1 अप्रैल को हुई। विक्रम संवत 2079 शुरू होने पर बधाइयों का तॉंता लग गया। वाट्ए एप और फेसबुक पर नववर्ष की धूम मच गई और अखबारों में एक कॉलम नए वर्ष पर अनिवार्यत: छापने की रस्म-अदायगी की गई। सभी जगह इसे हिंदू-नववर्ष कहा गया। हिंदू-नववर्ष इतना चला कि लोग भूल गये कि यह समय की गणना का एक तरीका है जिसे विक्रम संवत कहते हैं । संसार के अन्य स्थानों पर भी समय की गणना करने के प्रयास किये गये। ऋतुओं के आने का समय पता लगाने और उसी के अनुसारकृषि कार्य करने, मौसम के अनुरूप हवाओं की दिशाओं के अनुसार नौपरिवहन करने, त्यौहार पर्वों को नियत दिन पर मनाने और भूतकाल की घटनाओं को समय के पैमाने पर चिह्नित करने के लिए यह ज्ञान होना आवश्यक था।
प्रारंभ में विज्ञान का विकास नहीं हुआ था इसलिए विश्व के अधिकांश प्रारंभिक कैलेंडर बगैर किसी सिद्धांत के मात्र अनुभव के आधार पर बने थे । जूलियन कैलेंडर 10 माह का होता था जबकि रोमन कैलेंडर में 304 दिन होते थे। भारत के ही विभिन्न भागों में 36 से अधिक कैलेंडर प्रचलित थे जिनमें से अधिकतर अब प्रचलन से बाहर हैं। स्वाभाविक है यह वास्तविक सौर वर्ष या बदलती ऋतुओं के साथ संगति नहीं रख पाते थे इसलिए चलन से बाहर होते गये।
हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि समय की गणना का वैज्ञानिक तरीका सर्वप्रथम भारत में खोजा गया। ईसा से भी 1350 वर्ष पूर्व लिखे गयेमहात्मा लगध के ‘वेदांग ज्यातिष’ में चंद्रमास में दिनों की संख्या 29.53 बताई गई है जो वर्तमान वैज्ञानिक गणना के दशमलव के पहले अंक तक सही है। उन्होंने सौर वर्ष के दिनों की संख्या भी 366 बताई थी। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण दिन-रात होते हैं और मौसम बदलता हैं। भारत में यह हजारों वर्षों से मालूम था जबकि इसका पता पश्चिमी जगत को 16 वीं सदी में चला जब कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ ही साथ सूर्य का चक्कर भी लगाती है।
विक्रम संवत, ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के राजसिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इसमें काल गणना चंद्र मास पर आधारित है, परंतु सौर वर्ष के साथ व्यवहारिक संगति रखने के लिए समय-समय पर तिथियों का क्षय होता है (जैसे सप्तमी के बाद अष्टमी के स्थान पर सीधे नवमी आ जाए) अतिरिक्त माह (जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं) जोड़ा जाता है। सूर्य पर आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, सौर वर्ष पर आधारित है और मात्र साड़े चार सौ वर्ष पुराना है, परंतु अब सारे संसार में मानक कलैंडर के रूप में उपयोग हो रहा है।
यह सही है कि समय की गणना का वैज्ञानिक तरीका भारत में उन लोगों ने खोजा जो सनातन या हिंदू धर्म के अनुयायी थे परंतु इसका उपयोग केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। यह वैसा ही है जैसे शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5 वीं सदी में की थी, तो क्या शून्य को हम ‘हिंदू शून्य’ या ‘भारतीय शून्य’ कह सकते हैं ? उत्तर होगा – नहीं। मैक्स प्लांक ने सन 1900 में क्वांटम थ्योरी दी थी जिसने भौतिकी की मूल अवधारणा को ही बदल दिया। क्वांटम फिजिक्स की वर्तमान खोजों से यह धारणा बन रही है कि ब्रह्माण्ड के मूल की खोज करते करते विज्ञान उसी निष्कर्ष पर पहुँच रहा है जो भारतीय दर्शनों में पहले ही बताया जा चुका है कि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का स्रोत एक ही है। उसी स्रोत से कण बने हैं उसी से ऊर्जा। इसलिए दोनों आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। वही स्रोत चेतना के रूप में कण-कण में आभासित हो रहा है। उसी चेतना की अनुभूति कर लना ही अध्यात्म का चरम है। मैक्स प्लांक जर्मन ईसाई थे तो क्या हम क्वांटम थ्योरी को जर्मन या ईसाई क्वांटम थ्योरी कह सकते हैं ? उत्तर होगा नहीं। काल गणना के साथ भी यह सही है।
वेदों से जहॉं छ: धार्मिक दर्शनों (षड्दर्शन) – न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत – का विकास हुआ वहीं इसके साथ ही विज्ञान और कलाओं का विकास हुआ। विज्ञान और कलाओं की कुल संख्या 64है। इन्हें 6 अंगों में विभक्त किया गया है इसलिए इन्हें षडंगानि (छः अंग) कहते हैं। वेद के अंग होने के कारण यह वेदांग कहलाते हैं। वर्तमान शब्दावली में हम इन्हें धर्मनिरपेक्ष विज्ञान /कला कह सकते हैं। यह हैं – शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । कैलेंडर या पांचांग का निर्माण भी कलित ज्योतिष का हिस्सा है जो विज्ञान है और इसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है।
नव वर्ष उल्लास का अवसर है। भूतकाल से अनुभव लेकर भविष्य को सुखद बनाने का संकल्प है। इसलिए नववर्ष तभी होना चाहिए जब मनुष्यों के साथ ही प्रकृति भी प्रफुल्लित, उल्लासित हो। चैत्र माह में प्रकृति में नए सिरे से जीवन का प्रवाह होता है, वृक्षों में नए पत्ते आते हैं, मौसम आनंददायक होता है – न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, रबी की फसल पक जाती है, धन-धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में चैत्र माह से ज्यादा उपयुक्त अवसर नववर्ष की शुरूआत के लिए नहीं हो सकता। संसार में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी जलवायुवीय परिस्थितयॉं पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए वे देश अपना नववर्ष अलग तिथि को मनाते हैं । चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर नवदुर्गा की पूजा, उगादी, गुड़ी-पड़वा, चेटी चंड आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनकी अलग-अलग कथाऍं हैं परंतु एक बात एक सी है कि यह समय स्वाभविक रूप से ही उल्लास और उत्साह का होता है। नव वर्ष पर मनाए जाने वाले त्यौहार धार्मिक प्रथा का हिस्सा हैं परंतु नववर्ष की गणना पूरी तरह से वैज्ञानिक व प्रकृति के स्वरूप के आधार पर तय की गई है। हम धर्म और विज्ञान का व्यवहारिक धरातल पर अंतर जितनी अच्छी तरह समझ जाऍंगे धर्म और विज्ञान दोनों का उतना ही भला होगा।
इस प्रकार चैत्र प्रतिपदा का नववर्ष तो भारत भूमि पर रहनेवाले सब लोगों का नववर्ष है । इसे तो प्रकृति ने ही नववर्ष के रूप में तय किया है। हम हिंदू नववर्ष कहकर इसे संकुचित कर रहे हैं। जब हम इसे हिंदू नववर्ष कह देते हैं तो अन्य धर्मावलम्बी स्वाभाविक तौर पर इससे दूर हो जाते हैं। वेदों में सनातनधर्मियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे संसार के अन्यलोगों को आर्य अर्थात् श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव वाला बनाऍं (कृण्वन्तो विश्वमार्यम् – ऋग्वेद 9/63/5) । इसका अर्थ ही यह है उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान की खोजों से लाभन्वित करें। इसका दूसरा पक्ष यह है कि यदि अन्य लोगों ने कुछ अच्छा किया है तो उसे हम भी स्वीकार कर लाभान्वित हों। पश्चिम ने विज्ञान में जो तरक्की की है उसे अपनाने में हमने कभी संकोच नहीं किया । विज्ञान को धर्म, भाषा या नस्ल के आधार पर नहीं बॉंटा जा सकता। हमारा पांचांग मानव मात्र का है। इस पर गर्व कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भी विकास किया वह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से भावना से किया। उससे समस्त मानवमात्र को लाभान्वित होने दें। इसे हिंदुओं तक सीमित मत कीजिए।